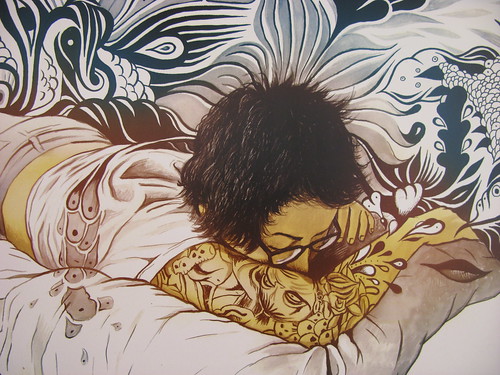दुनियाभर में 65 करोड़ लोग विकलांगता के शिकार हैं. वर्ष 2001 में हुई जनगणना के मुताबिक भारत में 2.19 करोड़ लोग विकलांग हैं जो कुल आबादी के 2.13 फ़ीसदी हैं. इसमें दृष्टि 29 फ़ीसदी श्रवण 6 फ़ीसदी, वाणी 7 फ़ीसदी, गति 28 फ़ीसदी और मानसिक 10 फ़ीसदी शामिल हैं. राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन (एनएसएसओ) के 2002 की रिपोर्ट के मुताबिक़ कुल विकलांगों में दृष्टि 14 फ़ीसदी श्रवण 15 फ़ीसदी, वाणी 10 फ़ीसदी, गति 51 फ़ीसदी और मानसिक 10 फ़ीसदी हैं. 75 फ़ीसदी विकलांग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, 49 फ़ीसदी विकलांग निरक्षर हैं और 34 फ़ीसदी रोज़गार प्राप्त हैं. पूर्व में चिकित्सकीय पुनर्वास पर दिए बल की बजाए अब सामाजिक पुनर्वास पर ध्यान दिया जा रहा है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांगता विभाग, विकलांग व्यक्तियों की मदद करता है, जिनकी संख्या वर्ष 2001 में हुई जनगणना के मुताबिक़ 2.19 करोड़ थी जो देश की कुल आबादी का 2.13 फ़ीसदी था. इनमें दृष्टि, श्रवण, वाणी, गति तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति शामिल थे.
हर साल 3 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है. 1981 से मनाए जा रहे इस दिन का मक़सद विकलांग व्यक्तियों के प्रति बेहतर समझ क़ायम करना और उनके अधिकारों पर ध्यान देने के साथ-साथ उन्हें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में मिलने वाले लाभ दिलाना है. विकलांगों से संबंधित विश्व कार्यकलाप कार्यक्रम ने विकलांगों की समाज में संपूर्ण और कारगर भागीदारी का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1982 में स्वीकार कर लिया. संयुक्त राष्ट्र ने विकलांगों के लिए पूर्ण और कारगर भागीदारी की प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसे 2006 में मंज़ूर विकलांगता के शिकार लोगों के नवगठित अधिकार समझौते में और मज़बूती प्रदान की गई. भारत ने 30 मार्च 2007 को संयुक्त राष्ट्र समझौते पर हस्ताक्षर किए. भारत सरकार विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी, उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. भारत की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है और स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवा तक पहुंच हमेशा से चुनौती का विषय रहा है. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों के ज़रिये उन लोगों तक पहुंचने के लिए अनेक क़दम उठाए हैं जिन तक पहुंचा नहीं जा सका.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हर साल 3 दिसम्बर को विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है. इन पुरस्कारों की शुरुआत 1969 में विकलांगों को नौकरी देने वाले सर्वश्रेष्ठ मालिकों और सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी को पुरस्कृत करने के लिए की गई थी. बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना की समीक्षा की गई और समय समय पर इसमें बदलाव करते हुए पुरस्कारों की विभिन्न नई श्रेणियां शुरू की गईं. राष्ट्रीय पुरस्कारों की वर्तमान योजना के मुताबिक़ विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए 13 श्रेणियों में 63 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी/ स्व रोज़गार विकलांग, सर्वश्रेष्ठ मालिक और नौकरी देने वाले अधिकारी/विकलांगों को नौकरी देने वाली एजेंसी, विकलांगों के लिए काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और संस्थान, अनुकरणीय व्यक्ति, विकलांगों का जीवन बेहतर बनाने के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक अनुसंधान/नवपरिवर्तन/उत्पादों का विकास, विकलांगों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण तैयार करने की दिशा में श्रेष्ठ कार्य, पुनर्वास सेवाएं देने वाला श्रेष्ठ ज़िला, राष्ट्रीय विश्वास की स्थानीय स्तर की समिति, राष्ट्रीय विकलांगता, वित्त् और विकास निगम को दिशा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ सृजनशील वयस्क विकलांग व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ सृजनशील विकलांग बच्चा, सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस और सर्वश्रेष्ठ सुगम्य वेबसाइट शामिल हैं.
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक़ देशभर के विभिन्न प्राधिकारों को पत्र लिखकर नामांकन मांगे गए. इसके अलावा मंत्रालय की वेबसाइट में विज्ञापन देने के अलावा देशभर के विभिन्न लोकप्रिय क्षेत्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में भी विज्ञापन दिये गए. जो सिफ़ारिशें प्राप्त हुईं उनमें से स्क्रीनिंग समिति ने संक्षिप्त सूची तैयार की और राष्ट्रीय चयन समिति ने पुरस्कारों को अंतिम रूप दिया. हर साल 3 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिए जाते हैं., भारतीय पुनर्वास परिषद् के मुताबिक़ निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को अनेक अधिकार दिए गए हैं. अविकलांग व्यक्तियों की तरह समान अवसर का अधिकार, विकलांगजनों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा और जीवन के कार्यों में अविकलांग व्यक्तियों के बराबर पूर्ण भागीदारी का अधिकार दिया गया है. इस अधिनियम द्वारा विकलांगजनों को क़ानूनी तौर पर मान्यता दी गई है और विभिन्न विकलांगताओं को क़ानूनी परिभाषा दी गई है.
इस अधिनियम से विकलांगजनों को यह अधिकार है कि उनकी देखभाल की जाए और जीवन की मुख्यधारा में उन्हें पुनर्वासित किया जाए और सरकार तथा इस अधिनियम द्वारा कवर किए गए प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरण और स्थापनाओं का यह दायित्व है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनज़र विकलांगजनों के प्रति अपने कर्त्तव्यों को पूरा करें. केन्द्रीय और राज्य सरकारों का यह कर्त्तव्य है कि वे रोकथाम संबंधी उपाय करें, ताकि विकलांगताओं को रोका जा सके. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें, स्वास्थ्य और सफ़ाई संबंधी सेवाओं में सुधार करें. वर्ष में कम से कम एक बार बच्चों की जांच करें, जोखिम वाले मामलों की पहचान करें. प्रसवपूर्व और प्रसव के बाद मां और शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल करें और विकलांगता की रोकथाम के लिए विकलांगता के कारण और बचाव के उपायों के बारे में जनता को जागरूक करें. प्रत्येक विकलांग बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है.
सरकार को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष स्कूल स्थापित करने चाहिए, सामान्य स्कूलों में विकलांग छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए और विकलांग बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अवसर मुहैया कराने चाहिए. पांचवीं कक्षा तक पढाई कर चुके विकलांग बच्चे मुक्त स्कूल या मुक्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से अंशकालिक छात्रों के रुप में अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं और सरकार से विशेष पुस्तकें और उपकरणों को निःशुल्क प्राप्त करने का उन्हें अधिकार है. सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह नए सहायक उपकरणों, शिक्षण सहायक साधनों और विशेष शिक्षण सामग्री का विकास करे ताकि विकलांग बच्चों को शिक्षा में समान अवसर प्राप्त हों. विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हैं, विस्तृत शिक्षा संबंधी योजनाएं बनानी हैं. विकलांग बच्चों को स्कूल जाने-आने के लिए परिवहन सुविधाएं देनी हैं, उन्हें पुस्तकें, वर्दी और अन्य सामग्री, छात्रवृत्तियां, पाठ्यक्रम और नेत्रहीन छात्रों को लिपिक की सुविधाएं देना है. दृष्टिहीनता, श्रवण विकलांग और प्रमस्तिष्क अंगघात से ग्रस्त विकलांगजनों की प्रत्येक श्रेणी के लिए पदों का आरक्षण होगा. इसके लिए प्रत्येक तीन वर्षों में सरकार द्वारा पदों की पहचान की जाएगी. भरी न गई रिक्तियों को अगले साल के लिए ले जाया जा सकता है.
विकलांगजनों को रोजगार देने के लिए सरकार को विशेष रोज़गार केन्द्र स्थापित करने हैं. सभी सरकारी शैक्षिक संस्थान और सहायता प्राप्त संस्थान सीटों को विकलांगजनों के लिए आरक्षित रखेंगे. रिक्तियों को गरीबी उन्मूलन योजनाओं में आरक्षित रखना है. नियोक्ताओं को प्रोत्साहन भी देना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा लगाए गए कुल कर्मचारियों में से 5 व्यक्ति विकलांग हैं. आवास और पुनर्वास के उद्देश्यों के लिए विकलांग व्यक्ति रियायती दर पर जमीन के तरजीही आबंटन के हक़दार होंगे. विकलांग व्यक्तियों के साथ परिवहन सुविधाओं, सड़क पर यातायात के संकेतों या निर्मित वातावरण में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. सरकारी रोजगार के मामलों में विकलांग व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा. सरकार विकलांग व्यक्तियों या गंभीर विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के संस्थानों की मान्यता निर्धारित करेगी. मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित शिकायतों के मामलों की जांच करेंगे. सरकार और स्थानीय प्राधिकरण विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य करेंगे, गैर-सरकारी संगठनों को सहायता देंगे, विकलांग कर्मचारियों के लिए बीमा योजनाएं बनाएंगे और विकलांग व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना भी बनाएंगे. छलपूर्ण तरीक़े से विकलांग व्यक्तियों के लाभ को लेने वालों या लेने का प्रयास करने वालों को 2 साल की सज़ा या 20 हज़ार रुपए तक का जुर्माना होगा.
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को भी अनेक अधिकार दिए गए हैं. इस अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार का यह दायित्व है कि वह ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए, नई दिल्ली में राष्ट्रीय न्यास का गठन करें. केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय न्यास को यह सुनिश्चित करना होता है कि इस अधिनियम की धारा 10 में वर्णित उद्देश्यों पूरे हों. राष्ट्रीय न्यास के न्यासी बोर्ड का यह दायित्व है कि वे वसीयत में उल्लिखित किसी भी लाभग्राही के समुचित जीवन स्तर के लिए आवश्यक प्रबंध करें और विकलांगजनों के लाभ हेतु अनुमोदित कार्यक्रम करने के लिए पंजीकृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करें. इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों को स्थानीय स्तर की समिति द्वारा नियुक्त संरक्षक की देखरेख में, रखे जाने का अधिकार है. नियुक्त किए गए ऐसे संरक्षकों उस व्यक्ति और विकलांग प्रतिपाल्यों की संपत्ति के लिए ज़िम्मेदार और उत्तरदायी होंगे.
यदि विकलांग व्यक्ति का संरक्षक उसके साथ दुप्र्यवहार कर रहा है या उसकी उपेक्षा कर रहा है या उसकी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है तो विकलांग व्यक्ति को अपने संरक्षक को हटा देने का अधिकार है. जहां न्यासी बोर्ड कार्य नहीं करता या इसने सौंपे गए कार्यों के कार्यनिष्पादन में लगातार चूक की है, वहां विकलांग व्यक्तियों हेतु पंजीकृत संगठन, न्यासी बोर्ड को हटाने/इसका पुनर्गठन करने के लिए केन्द्रीय सरकार से शिकायत कर सकता है. इस अधिनियम के उपबन्ध राष्ट्रीय न्यास पर जवाबदेही, मॉनीटरिग, वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा के मामले में बाध्यकारी होंगे.
भारतीय पुनर्वास अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को भी अधिकार दिए गए हैं. इस अधिनियम के तहत परिषद द्वारा रखे जा रहे रजिस्टरों में जिन प्रशिक्षित और विशेषज्ञ व्यावसायिकों के नाम दर्ज हैं, उनके द्वारा विकलांगजनों को लाभ पहुंचाना. शिक्षा के उन न्यूनतम मानकों को बनाए रखने की गारंटी जो भारत में विश्वविद्यालयों या संस्थानों द्वारा पुनर्वास अर्हता की मान्यता के लिए अपेक्षित हैं. शिक्षा के उन न्यूनतम मानकों को बनाए रखने की गारंटी जो भारत में विश्वविद्यालयों या संस्थानों द्वारा पुनर्वास अर्हता की मान्यता के लिए अपेक्षित हैं. केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन और अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर किसी सांविधिक परिषद द्वारा पुनर्वास व्यावसायिकों के व्यवसाय के विनियम की गारंटी.
मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अंतर्गत विकलांगों को अनेक अधिकार दिए गए हैं. मानसिक रुप से रुग्ण व्यक्तियों के उपचार और देखभाल के लिए सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किए जा रहे किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय नर्सिग होम या स्वास्थ्य लाभ गृह (सरकारी सार्वजनिक अस्पताल या नर्सिग होम के अलावा) में भर्ती होने, उपचार करवाने या देखभाल करवाने का अधिकार. मानसिक रुप से रुग्ण कैदी और नाबालिग को भी सरकारी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय नर्सिग होम्स में इलाज करवाने का अधिकार है. 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों, व्यवहार में परिवर्तन कर देने वाले अल्कोहल या अन्य व्यवसनों के आदी व्यक्ति और वे व्यक्ति जिन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, को सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किए जा रहे अलग मनश्चिकित्सीय अस्पतालों या नर्सिग होम में भर्ती होने, उपचार करवाने या देखरेख करवाने का अधिकार है. मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों को सरकार से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को विनियमित, निर्देशित और समन्वित करवाने का अधिकार है.
सरकार का दायित्व इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय प्राधिकरणों और राज्य प्राधिकरणों के माध्यम से मनश्चिकित्सीय अस्पतालों और नर्सिग होमों को स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए ऐसे विनियमनों और लाइसेंसों को जारी करने का है. इन सरकारी अस्पतालों और नर्सिग होमों में इलाज अन्तःरोगी या बाह्य रोगी के रुप में हो सकता है. मानसिक रुप से रुग्ण व्यक्ति ऐसे अस्पतालों या नर्सिग होमों में अपने आप भर्ती होने के लिए अनुरोध कर सकते हैं और नाबालिग अपने संरक्षकों के द्वारा भर्ती होने के लिए अनुरोध कर सकते हैं. मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के रिश्तेदारों द्वारा भी रुग्ण व्यक्तियों की ओर से भर्ती होने के लिए अनुरोध किया जा सकता है. भर्ती आदेशों को मंज़ूर करने के लिए स्थानीय मजिस्ट्रेट को भी आवेदन किया जा सकता है. पुलिस का दायित्व है कि भटके हुए या उपेक्षित मानसिक रुग्ण व्यक्ति को सुरक्षात्मक हिफाजत में लें, उसके संबंधी को सूचित करें और ऐसे व्यक्ति के भर्ती आदेशों को जारी करवाने हेतु उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करें.
मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों को इलाज होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने का अधिकार है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वह छुट्टी का हक़दार है. जहां कहीं मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति भूमि सहित अपनी अन्य संपत्तियों की स्वयं देखरेख नहीं कर सकते वहां, जिला न्यायालय आवेदन करने पर ऐसी संपत्तियों के प्रबंधन की रक्षा और सुरक्षा ऐसे मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के संरक्षकों की नियुक्ति करने के द्वारा या ऐसी संपत्ति के प्रबंधकों की नियुक्ति द्वारा प्रतिपालय न्यायालय को सौंप कर करनी पड़ती है. सरकारी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या नर्सिग होम में अंतःरोगी के रूप में भर्ती हुए मानसिक रुप से रुग्ण व्यक्ति के उपचार का ख़र्च, जब तक कि मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति की ओर से उसके संबंधी या अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे ख़र्च को वहन करने की सहमति न दी गई हो, संबंधित राज्य सरकार द्वारा ख़र्च का वहन किया जाएगा और इस तरह के अनुरक्षण के लिए प्रावधान ज़िला न्यायालय के आदेश द्वारा दिए गए हैं. इस तरह का खर्च मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति की संपत्ति से भी लिया जा सकता है. इलाज करवा रहे मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का असम्मान (चाहे यह शारीरिक हो या मानसिक) या क्रूरता नहीं की जाएगी और न ही मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति का प्रयोग उसके रोग-निदान या उपचार को छोड़कर, अनुसंधान के उद्देश्य से या उसकी सहमति से नहीं किया जाएगा. सरकार से वेतन, पेंशन, ग्रेच्यूटी या अन्य भत्तों के हकदार मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों (जैसे सरकारी कर्मचारी, जो अपने कार्यकाल के दौरान मानसिक रूप से रुग्ण हो जाते हैं), को ऐसे भत्तों की अदायगी से मना नहीं किया जा सकता है. मजिस्ट्रेट से इस आशय का तथ्य प्रमाणित होने के बाद, मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति की देखरेख करने वाला व्यक्ति या मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति के आश्रित ऐसी राशि को प्राप्त करेंगे. यदि मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति कोई वकील नहीं कर सकता या कार्यवाहियों के संबंध में उसकी परिस्थितियों की ऐसी अपेक्षा हो तो अधिनियम के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट या ज़िला न्यायालय के आदेश द्वारा वकील की सेवाओं को लेने का अधिकार है.
विकलांगों के कल्याण के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. विकलांगों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 500 नई छात्रवृत्ति ऐसे प्रतिभागियों को दी जाती है जो 10वीं के बाद 1 साल से अधिक अवधि वाले व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करते हैं. हालांकि मानसिक पक्षाघात, मानसिक मंदता, बहु-विकलांगता तथा गंभीर श्रवण हानि से ग्रस्त छात्रों की स्थिति में छात्रवृत्ति 9वीं कक्षा से छात्र-छात्राओं को अध्ययन पूरा करने के लिए दी जाती है. छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थनापत्र आमंत्रित करने की विज्ञप्ति प्रमुख राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचारपत्रों में जून के महीने में दी जाती है तथा इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाता है. राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से इस योजना के व्यापक विज्ञापन के लिए अनुरोध किया जाता है.
ऐसे छात्र जो 40 फ़ीसदी या ज़्यादा विकलांग की श्रेणी में आते हैं और जिनके परिवार की आय 15 हज़ार रुपए से ज़्यादा न हो, वे भी इस योजना के तहत आते हैं. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों वाले छात्रों को प्रति माह 700 रुपए की राशि सामान्य स्थिति में तथा 1,000 रुपए की राशि छात्रावास में रहने वाले छात्रों को दी जाती है. डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों वाले छात्रों को प्रति माह 400 रुपए की राशि सामान्य स्थिति में तथा 700 रुपए की राशि छात्रावास में रहने वाले छात्रों को दी जाती है. छात्रवृत्ति के अलावा छात्रों को पाठ्यक्रम की फ़ीस भी दी जाती है जिसकी राशि वार्षिक 10,000 रुपए तक है. इस योजना के तहत अंधे /बहरे स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए सॉफ्ट्वेयर के साथ कंप्यूटर के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है. यह सहायता मानसिक पक्षाघात से ग्रस्त छात्रों को आवश्यक सॉफ्टवेयर की उपलब्धता के लिए भी दी जाती है.
सिर्फ़ योजनायें बनाने से विकलांगों का सशक्तिकरण होने वाला नहीं है. इसके लिए ज़रूरी है कि सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे. इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है. आम लोगों को भी चाहिए कि अगर उनके आस-पास ऐसा कोई व्यक्ति या बच्चा है तो उसके परिजनों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मुहैया कराएं. यक़ीन मानिए हमारी ज़रा सी मदद से किसी की ज़िन्दगी की दिशा बदल सकती है. उसे जीने की एक नई राह मिल सकती है. मौक़ा मिलने पर विकलांग व्यक्ति भी विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी की इबारत लिख सकते हैं.